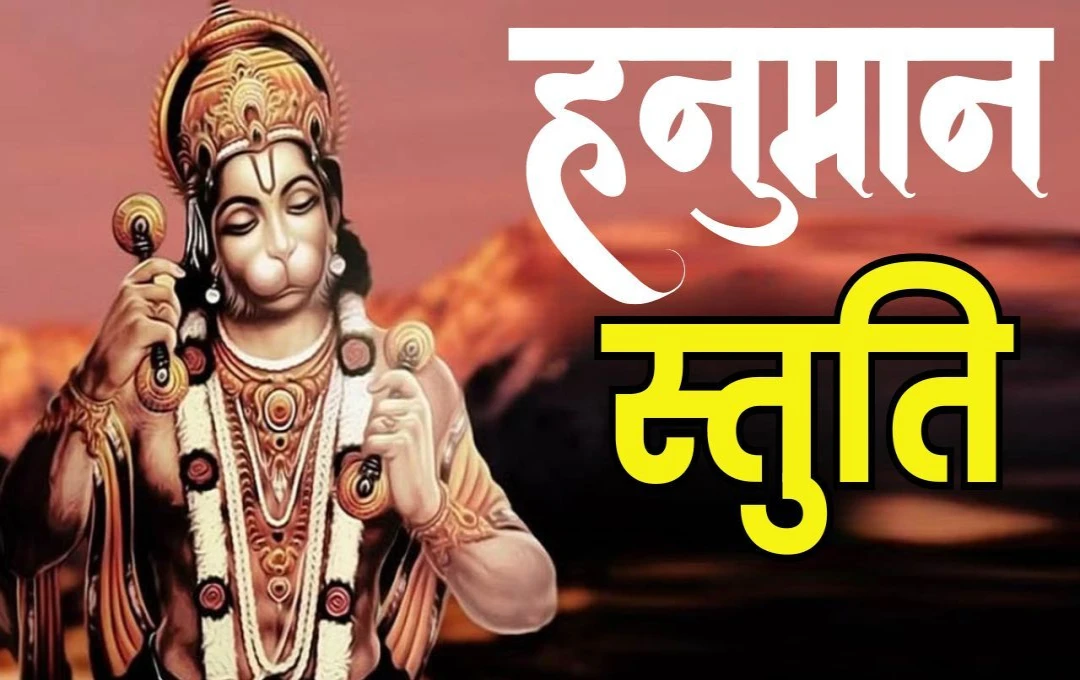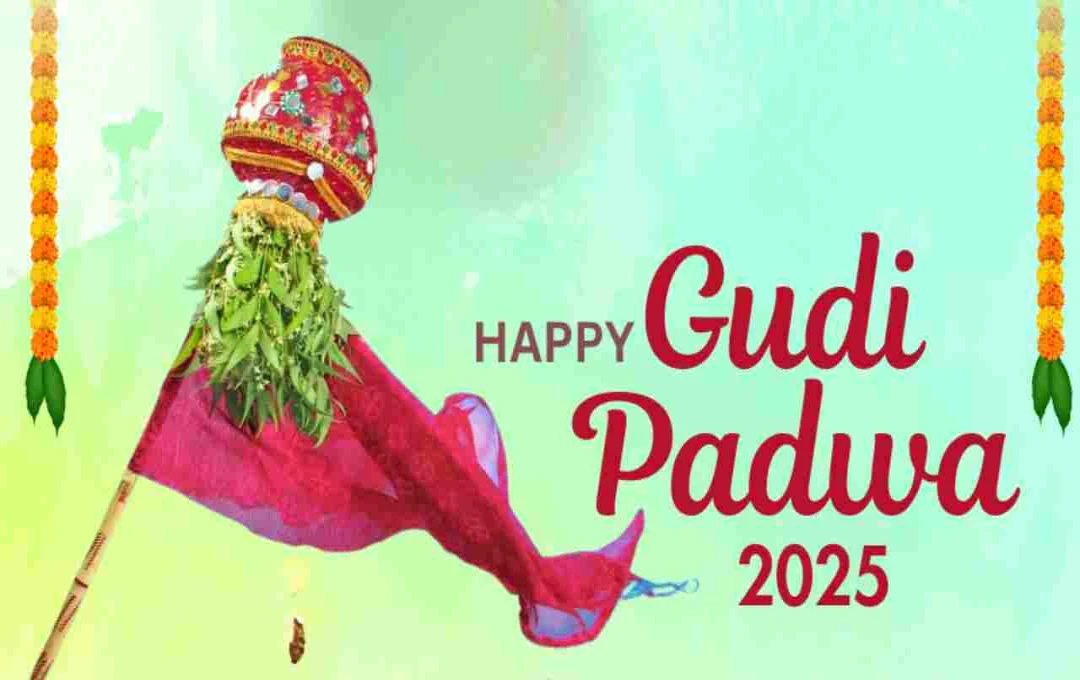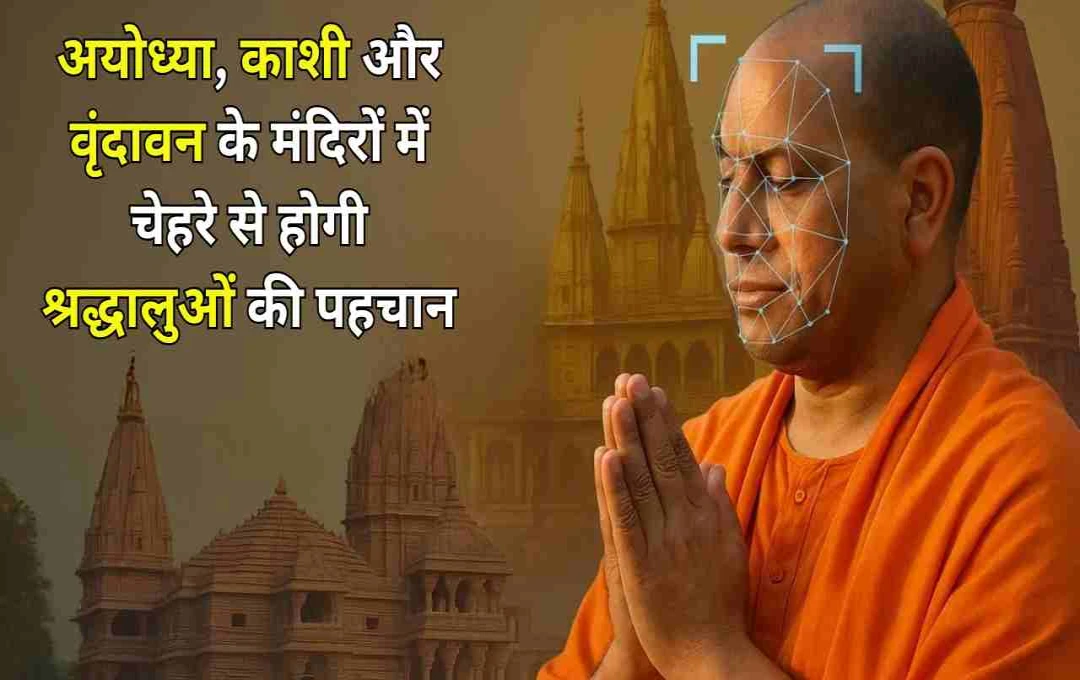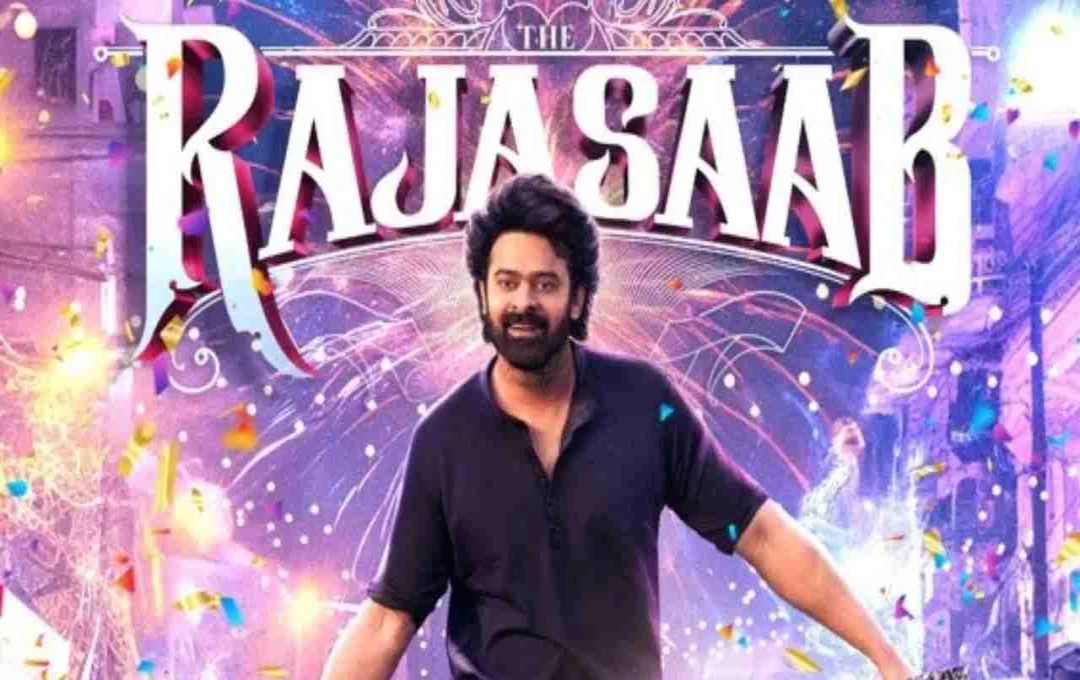आज जब देशभर में श्रद्धालु राम नवमी का पर्व मना रहे हैं, तो यह जानना भी रोचक है कि भगवान राम की कथा सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ तक सीमित नहीं रही। बीते 2400 वर्षों में हर शताब्दी में किसी न किसी रूप में रामकथा का निर्माण हुआ है। न सिर्फ भारत, बल्कि दुनिया के 9 से ज्यादा देशों में रामायण की अलग-अलग रूपों में रचना की गई है। हैरानी की बात यह भी है कि मुगल शासक अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने भी रामायण का फारसी और उर्दू में अनुवाद करवाया था।
फादर कामिल बुल्के: एक विदेशी जिसने राम में पाया जीवन का सार
फादर कामिल बुल्के एक बेल्जियम से आए ईसाई मिशनरी थे, लेकिन भारत आने के बाद उन्होंने यहां की संस्कृति और खासकर रामकथा में गहरी रुचि दिखाई। साल 1935 में जब वे भारत आए, तो उन्होंने तुलसीदास की 'रामचरितमानस' पढ़ी और उससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस ग्रंथ को अपने जीवन का केंद्र बना लिया। हिंदी भाषा के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया, जहां से उन्होंने हिंदी साहित्य में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की।
फादर बुल्के ने अपने शोध में ‘रामकथा का विकास’ नामक पुस्तक लिखी, जो आज भी रामकथा पर सबसे गहराई से लिखी गई और प्रमाणिक पुस्तकों में मानी जाती है। उन्होंने वाल्मीकि रामायण से लेकर तुलसीदास की मानस और अन्य लोक परंपराओं में फैली रामकथाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया। उनका काम यह दिखाता है कि एक विदेशी होकर भी उन्होंने भारतीय संस्कृति को दिल से अपनाया और राम के आदर्शों में जीवन का सार देखा।
वाल्मीकि रामायण: सबसे प्राचीन, लेकिन राम का उल्लेख उससे पहले भी

जब भी रामकथा की बात होती है, तो सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि की रामायण का नाम आता है। माना जाता है कि उन्होंने ही रामकथा को सबसे पहले विस्तार से लिखा। लेकिन राम का नाम इससे भी पहले के ग्रंथों में मिलता है। ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद माना जाता है, उसमें भी ‘राम’ नाम का जिक्र है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ऋग्वेद में जिस राम का उल्लेख है, वे वही भगवान राम हैं या कोई और धार्मिक और प्रतापी राजा। फिर भी यह दिखाता है कि "राम" नाम का महत्व बहुत पुराना है।
रामकथा का सबसे पहला व्यवस्थित वर्णन बौद्ध ग्रंथ ‘दशरथ जातक’ में मिलता है, जो ईसा से लगभग 400 साल पहले लिखा गया था। इस ग्रंथ में राम, लक्ष्मण और सीता का वर्णन है। इसके करीब 100 साल बाद महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण की रचना की, जो आज सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित रामकथा मानी जाती है। खास बात यह है कि वाल्मीकि को राम और सीता का समकालीन माना गया है। कहा जाता है कि राम और सीता के पुत्र लव-कुश ने ही वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को राम के दरबार में गाया था।
रामायणों का समंदर: 400 से ज्यादा वर्जन, 3000 से अधिक ग्रंथों में राम का जिक्र
रामकथा का समंदर अत्यंत विशाल है, जिसमें 400 से ज्यादा रामकथाओं के विभिन्न रूप पाए जाते हैं। फादर बुल्के के शोध के अनुसार, इन रामकथाओं का प्रसार न केवल भारतीय भाषाओं में है, बल्कि विश्वभर में कई विदेशी भाषाओं में भी रामकथा के अनेक रूप मौजूद हैं। संस्कृत, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, असमिया, मलयालम जैसी भारतीय भाषाओं के अलावा डच, अंग्रेजी, फ्रेंच, फारसी, उर्दू और थाई जैसी भाषाओं में भी रामकथा की व्यापकता है।
रामायणों का यह विविधता भरा संसार न केवल धर्म और संस्कृति का संग्रह है, बल्कि प्रत्येक संस्करण ने रामकथा को अपने समाज और संस्कृति के अनुसार नया रूप दिया है। जैसे वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, रामचरितमानस, रंगनाथ रामायण, कंब रामायण, कृतिवास रामायण और सेरीराम रामायण— इन सभी ग्रंथों में राम की कथा के अलग-अलग दृष्टिकोण और भाषाई विशेषताएं हैं, जो इस महान कथा को वैश्विक रूप से एक अमूल्य धरोहर बनाती हैं।
कुछ अनसुनी कहानियां: जब सीता ने हनुमान को आम दिए और कंगन बेचे

आनंद रामायण में एक दिलचस्प और मानवीय कथा का वर्णन है, जिसमें सीता जी ने हनुमान जी को अपने हाथ के कंगन दिए और उन्हें आम भी दिए। यह घटना तब की है जब हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता से मिलने के बाद बहुत भूखे हो जाते हैं। सीता जी ने देखा कि हनुमान जी को खाने की जरूरत है, तो उन्होंने अपनी ओर से उनका भला करने का फैसला किया। सीता ने उन्हें अपने सुंदर कंगन दिए ताकि वे लंका के बाजार से फल खरीद सकें और अपना पेट भर सकें। इसके साथ ही सीता ने उन्हें दो आम भी दिए, जो उनके खाने के लिए थे।
इस प्रसंग में सीता का एक मानवीय रूप सामने आता है, जिसमें उनकी माँसिकता और संवेदनशीलता झलकती है। वह केवल एक देवी नहीं, बल्कि एक मां और एक स्त्री के रूप में भी अत्यधिक करुणा और प्रेम की प्रतीक हैं। यह दृश्य उनके समर्पण और त्याग की गहरी भावना को दर्शाता है, जो भगवान राम के प्रति उनके प्रेम को और भी मजबूत बनाता है।
रंगनाथ रामायण: हनुमान ने विभीषण के लिए बनाई थी नई लंका
रंगनाथ रामायण में एक रोचक और दिलचस्प घटना का वर्णन मिलता है, जब विभीषण को लंका का राजा घोषित किया गया। इसके बाद हनुमान जी ने विभीषण के लिए एक नई लंका बनाई, जिसे "हनुमत्लंका" या "सिकतोद्भव लंका" कहा गया। हनुमान ने बालू और रेत से यह नई लंका बनाई, ताकि विभीषण को एक मजबूत और सुरक्षित राज्य मिल सके। यह कार्य हनुमान जी की निष्ठा, समर्पण और विभीषण के प्रति उनके समर्थन को दर्शाता है।
इसके अलावा, कुछ ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि त्रिजटा, जो अशोक वाटिका में सीता की पहरेदारी करती थी, दरअसल विभीषण की बेटी थी। त्रिजटा सीता के प्रति मातृत्व भावना रखती थी और उन्हें अपनी मां जैसा मानती थी। यह प्रसंग भी रामायण की कहानियों में एक नया पहलू जोड़ता है, जो रिश्तों और संवेदनाओं की गहराई को उजागर करता है।
उर्दू और फारसी में भी रामकथा: अकबर से शाहजहां तक
16वीं सदी के बाद, भारत आए कई यूरोपीय यात्रियों ने रामकथा को अपने अनुभवों में दर्ज किया और उसे अपनी किताबों में लिखा। इन यात्रियों ने राम के जीवन, उनके संघर्षों और आदर्शों के बारे में अपनी समझ और विचार साझा किए।

1609 में, मिशनरी जे. फेनिचियो ने अपनी पुस्तक लिब्रो डा सैटा में राम के अवतार और रावण वध का वर्णन किया। उन्होंने रामकथा के मुख्य तत्वों को यूरोपीय पाठकों के लिए समझाया और भारतीय संस्कृति से उनका परिचय कराया।
1651 में, डच पादरी ए. रोजेरियुस ने द ओपन दोरे नामक किताब में रामायण के पूरे कथा क्रम को दर्शाया। इस किताब में राम के जीवन के प्रमुख घटनाओं को विस्तार से बताया गया, जिससे यूरोपियन पाठकों को भारतीय साहित्य और संस्कृति की एक झलक मिली।
1658 में, पी. बलडेयुस ने डच भाषा में आफगोडेरैय डर ओस्ट इण्डिशे हाइडेनन नामक ग्रंथ में राम के जीवन का विस्तार से वर्णन किया। इस ग्रंथ ने राम के आदर्श और उनके संघर्षों को एक नई नजर से प्रस्तुत किया।
18वीं सदी में, फ्रेंच यात्री एम. सोनेरा ने अपनी किताब बॉयाज ओस इण्ड ओरियंटल में राम को 15 वर्षीय योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास गए थे, जो भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
रामकथा की विदेश यात्रा: यूरोपीय लेखकों की नजर में राम
16वीं सदी के बाद भारत आने वाले कई यूरोपीय यात्रियों ने रामकथा को अपने अनुभवों में शामिल किया और उसे अपनी किताबों में लिखा। इनमें से कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं:
1609: मिशनरी जे. फेनिचियो ने अपनी पुस्तक ‘लिब्रो डा सैटा’ में राम के अवतार और रावण वध का वर्णन किया। उन्होंने रामकथा को पश्चिमी पाठकों के लिए सुलभ बनाने की कोशिश की और इस कथा के धार्मिक महत्व को भी बताया।
1651: डच पादरी ए. रोजेरियुस ने ‘द ओपन दोरे’ नामक पुस्तक में रामायण के पूरे कथा क्रम को दर्शाया। इसमें उन्होंने राम के जीवन के प्रमुख घटनाओं को विस्तार से बताया, जैसे राम का वनवास और रावण से युद्ध।
1658: पी. बलडेयुस ने डच भाषा में ‘आफगोडेरैय डर ओस्ट इण्डिशे हाइडेनन’ नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें राम के जीवन का विस्तार से वर्णन किया। इस ग्रंथ ने यूरोप में रामकथा को और भी प्रसिद्ध किया।
18वीं सदी: फ्रेंच यात्री एम. सोनेरा ने अपनी पुस्तक "बॉयाज ओस इण्ड ओरियंटल" में राम को 15 वर्षीय योद्धा बताया, जो अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास गया। उन्होंने राम को एक वीर योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया।
अध्यात्म रामायण में सीता का दिलचस्प तर्क

अध्यात्म रामायण में एक दिलचस्प प्रसंग है जब राम वनवास जाने के लिए तैयार होते हैं और सीता उन्हें छोड़ने की सोचती हैं। लेकिन सीता उनसे कहती हैं, 'मैंने जितनी भी रामकथाएं सुनी हैं, सभी में सीता राम के साथ वन जाती हैं। अगर आप मुझे छोड़ गए तो सब कुछ गलत हो जाएगा।' इस तर्क से राम मुस्कुरा उठते हैं और उन्हें वनवास के लिए साथ ले जाते हैं। यह कहानी दिखाती है कि सीता के मन में राम के प्रति गहरी निष्ठा और उनके साथ रहने की इच्छा थी, जिससे राम भी अंततः उनकी बात मानते हैं।
रामकथा: सिर्फ कथा नहीं, सांस्कृतिक विरासत
रामकथा सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका प्रभाव सिर्फ धार्मिक साहित्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कला, संगीत, नृत्य, चित्रकला और स्थापत्य में भी गहरे तरीके से महसूस होता है। उदाहरण के लिए, रामलीला जैसी पारंपरिक नृत्य नाटिकाओं में राम की कहानी जीवित रहती है, जहां कलाकार भगवान राम और उनके संघर्षों को मंच पर प्रस्तुत करते हैं। यह न केवल धार्मिक शिक्षा देती है, बल्कि समाज में धर्म, नैतिकता और आदर्शों के बारे में भी महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाती है।
इसके अलावा, रामकथा का प्रभाव भारत के बाहर भी देखा जा सकता है। इंडोनेशिया जैसे देशों में शैडो थिएटर, जिसे 'वायांग कुलित' कहते हैं, में रामकथा का अहम स्थान है। इस तरह की प्रस्तुतियों में राम और रावण के युद्ध की कथाएं बघाई जाती हैं, जो दर्शकों को धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा का अनुभव देती हैं। इस प्रकार, रामकथा न सिर्फ एक कहानी है, बल्कि यह भारतीय और एशियाई सभ्यताओं की सांस्कृतिक धरोहर का एक जीवंत प्रतीक है।
रामकथा एक जीवंत परंपरा है, जो सदियों से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। यह केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि संस्कृति, साहित्य, दर्शन और भावनाओं की साझा विरासत है। हर युग, हर समाज, हर भाषा ने इसे अपने-अपने तरीके से अपनाया और गढ़ा, जिससे राम सिर्फ एक पात्र नहीं, बल्कि बहुआयामी चेतना बन गए। रामनवमी पर इस अमर गाथा को जानना केवल श्रद्धा नहीं, अपने सांस्कृतिक इतिहास से जुड़ाव भी है।